सविनय अवज्ञा आन्दोलन- महत्त्व ,योगदान,परिणाम
B.A.I, Political Science II / 2020
प्रश्न 4. महात्मा गांधी
द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए एवं उसके
महत्त्व का विवेचन कीजिए।
प्रश्न 4. महात्मा गांधी
द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए एवं उसके
महत्त्व का विवेचन कीजिए।
अथवा '' भारत में
राष्ट्रीय चेतना के विकास में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का क्या योगदान है ? समझाइए।
अथवा '' महात्मा
गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन का वर्णन कीजिए। इसका क्या परिणाम
निकला?
उत्तर –
गांधीजी ने
अहिंसात्मक सिद्धान्तों के आधार पर सन् 1920-21 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन
प्रारम्भ किया था। इसके पश्चात् । देश की संवैधानिक समस्याओं को हल करने के लिए
सरकार की ओर से साइमन कमीशन भारत आया, उसकी रिपोर्ट निरर्थक थी। इसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने
सरकार को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए सरकार
को एक वर्ष का समय दिया। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर सन् 1929 के लाहौर
अधिवेशन में 31 दिसम्बर की
रात्रि को 12 बजे सभी
कार्यकर्ताओं ने रावी नदी के तट पर तिरंगे झण्डे के नीचे 'पूर्ण स्वराज्य' की शपथ ली। इस
अधिवेशन में 31 दिसम्बर को
पूर्ण स्वराज्य की माँग के सम्बन्ध में प्रस्ताव इस प्रकार पारित हुआ, "वर्तमान
परिस्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना बेकार है। कांग्रेस के
संविधान की प्रथम धारा में 'स्वराज्य' शब्द का अभिप्राय पूर्ण स्वाधीनता से है। यह कांग्रेस
अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को अधिकार देता है कि वह जब भी ठीक समझे, सविनय अवज्ञा
आन्दोलन प्रारम्भ कर दे, जिसमें करों का न
देना भी शामिल है।"
· सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने के कारण
सविनय अवज्ञा
आन्दोलन प्रारम्भ करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे
(1) सरकार ने सन् 1928 की नेहरू समिति
की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था।
(2) भारत को
औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने से मना कर दिया था।
(3) विश्व मन्दी के कारण किसानों व मजदूरों की दशा बिगड़ चुकी
थी और उनमें साम्यवादी विचारों का उदय हो रहा था, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस को कदम उठाना
आवश्यक था।
(4) सन् 1928 में बारदोली (सूरत जिला) में सरदार पटेल ने भूमि कर न देने
से सम्बन्धित आन्दोलन का सफल प्रयोग कर लिया था।
(5) उपर्युक्त के अतिरिक्त गांधीजी ने यह अनुभव किया कि यदि देश
में स्वाधीनता के लिए शीघ्र ही शान्तिपूर्ण व अहिंसक आन्दोलन न चलाया गया, तो देश में
हिंसात्मक क्रान्ति की सम्भावना है।
सविनय अवज्ञा आन्दोलन का कार्यक्रम
सविनय अवज्ञा आन्दोलन
आरम्भ करने से पहले महात्मा गांधी ने अपनी 11 माँगों की एक सूची तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजी
थी। यह सूची आन्दोलन का कार्यक्रम था
(1) सम्पूर्ण मदिरा निषेध।
(2) विनिमय की दर में
कमी करके एक शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए।
(3) भूमि का लगान आधा
हो और उस पर कौंसिल का नियन्त्रण रहे।
(4) नमक कर समाप्त कर
दिया जाए।
(5) सेना का खर्च आधा
कर दिया जाए।
(6) बड़ी-बड़ी सरकारी
नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए।
(7) विदेशी वस्त्रों
के आयात पर निषेध कर लगे।
(8) भारतीय समुद्र तट
भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहें।
(9) सभी राजनीतिक
कैदियों को रिहा कर दिया जाए और राजनीतिक मामले खत्म कर दिए जाएँ।
(10) गुप्तचर पुलिस को या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर जनता
का नियन्त्रण रहे।
(11) आत्म-रक्षा के लिए हथियार रखने के लाइसेंस दिए जाएँ।
इन माँगों के सन्दर्भ में
लॉर्ड इरविन का उत्तर निराशाजनक रहा। इस पर गांधी ने कहा कि "हमने माँगी थी
रोटी, परन्तु मिले
पत्थर। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। भारत एक विशाल जेलखाना है।
मैं इन ब्रिटिश कानूनों को व्यर्थ समझता हूँ और मैं इस शोकमय शान्ति को भंग करना
चाहता हूँ, जो राष्ट्र के
दिल को कष्ट दे रही है।"
· सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ तथा प्रगति
डाण्डी यात्रा इस आन्दोलन
का प्रारम्भ 12 मार्च, 1930 को गांधीजी की
डाण्डी यात्रा से हुआ। गांधीजी ने अपने 78 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने और उसे
चुनौती देने के लिए गुजरात प्रदेश के समुद्र तट पर स्थित डाण्डी नामक स्थान की ओर
नमक कानून तोड़ने के लिए कूच किया। साबरमती आश्रम से डाण्डी समुद्र तट तक 200 मील की पैदल
यात्रा 24 दिन में पूरी हुई।
6 अप्रैल, 1930 को प्रात:काल की
प्रार्थना के पश्चात् गांधीजी ने डाण्डी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा
और आन्दोलन का श्रीगणेश किया।
नमक कानून तोड़ने के
अलावा इस आन्दोलन के अन्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं
(1) जनता सरकार को कर नहीं देगी।
(2) वह ऐसे कानूनों को नहीं मानेगी जो आत्म-निर्णय के सिद्धान्त
के विरुद्ध हों।
(3) विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए।
(4) शराब की दुकानों
पर धरना दिया जाए।
(5) विद्यार्थियों
द्वारा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए।
(6) सरकारी कर्मचारी
दफ्तरों को छोड़ दें।
गांधीजी के आह्वान पर
पूरे देश की जनता ने इस आन्दोलन में भाग लिया। सरकार के अनुचित कानूनों का सर्वत्र
उल्लंघन किया गया। खादी निर्माण कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर चलाया गया, जिससे 1 लाख व्यक्तियों
को रोजगार मिल गया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। इस आन्दोलन में स्त्रियों ने
सबसे अधिक उत्साह से भाग लिया। अकेले दिल्ली में ही 1,700 महिलाएँ शराब की
दुकानों पर धरना देती हुई बन्दी बनाई गईं।
सरकार की दमन
नीति - आन्दोलन के प्रभाव और प्रगति को देखकर ब्रिटिश
सरकार स्तब्ध रह गई। उसने दमन नीति का प्रयोग किया। लाखों व्यक्तियों को बन्दी
बनाया गया। निहत्थे सत्याग्रहियों पर लाठी प्रहार किया गया। सबसे भयंकर लाठी
प्रहार धरासना में नमक के गोदाम पर धरना देने वाले 2,500 निहत्थे स्वयंसेवकों पर किया गया। इस विषय में
पट्टाभि सीतारमैय्या लिखते हैं
"जमीन पीड़ा से कराहते हुए मनुष्यों से पट गई।
लोगों के कपड़े खून से तर हो गए। स्वयंसेवकों का अनुशासन देखने योग्य था। उनके
रोम-रोम में अहिंसा बसी हुई थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने गांधीजी की अहिंसा को
घोलकर पी लिया हो।"
16 अप्रैल, 1930 को पं. जवाहरलाल नेहरू और 4 मई को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। फलतः
आन्दोलन और भी अधिक तीव्र हो गया।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन (नवम्बर, 1930) -
इधर भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल रहा था, उधर भारत की संवैधानिक गुत्थी को सुलझाने के लिए 12 नवम्बर, 1930 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रैम्जे मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में लन्दन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। इसमें भाग लेने के लिए 89 प्रतिनिधियों में से 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश संसद के, 16 भारतीय रियासतों के, शेष 57 ब्रिटिश भारत के थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा साम्प्रदायिक समस्या पर भी विचार-विमर्श हुआ।सम्मेलन की असफलता और गांधी-इरविन समझौता (1931) -
19 जनवरी, 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना निर्णय पर पहुँचे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह अनुभव किया कि कांग्रेस के बिना भारत की राजनीतिक गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सकता। अत: सरकार ने कांग्रेस से सहयोग करने के लिए प्रयत्न किया। कांग्रेस पर से पाबन्दी हटा ली गई व कांग्रेस के नेताओं को बिना किसी शर्त रिहा कर दिया गया। उधर सर तेज बहादुर सप्रू व डॉ. जयकर जैसे नेताओं ने गांधीजी को परामर्श दिया कि यदि वे सरकार के साथ वार्ता में शामिल नहीं होंगे, तो सरकार रियासतों के नरेशों और मुसलमानों से कोई समझौता कर सकती है, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। इन नेताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप गांधीजी व इरविन में वार्ता प्रारम्भ हुई और मार्च, 1931 में दोनों में एक समझौता हुआ, जिसे 'गांधी-इरविन समझौता' कहा जाता है। समझौते के तहत गांधीजी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (सितम्बर, 1931) -
7 सितम्बर, 1931 को लन्दन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। गांधीजी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12 सितम्बर को लन्दन पहुँचे। इस सम्मेलन के प्रारम्भ होने तक ब्रिटेन व भारत में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। मजदूर दल की सरकार का पतन हो चुका था और राष्ट्रीय सरकार बनी थी। अनुदारवादी दल का प्रभुत्व बढ़ चुका था। अनुदार दल के सेमुअल होर भारत मन्त्री बने और लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड विलिंगडन को वायसराय नियुक्त किया गया। ये दोनों ही बहुत प्रतिक्रियावादी विचारों के थे। उधर सम्मेलन में गांधीजी को छोड़कर अन्य किसी भी भारतीय प्रतिनिधि ने भारत के लिए स्वतन्त्रता की माँग नहीं की। सभी अपनी जातियों के लिए विशेष रियासतों की माँग करते रहे। फलतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसम्बर, 1931 को बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। गांधीजी लन्दन से खाली हाथ लौटे।सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पुनरावृत्ति (1932-34) -
जब गांधीजी स्वदेश लौटे, तो पहले से निश्चित क्रूर अध्यादेशों को वायसराय विलिंगडन ने लागू कर दिया। कांग्रेस को पुनः अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। पं. नेहरू, खान अब्दुल गफ्फर खाँ आदि प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। अत: कार्य समिति ने अनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का निश्चय किया। गांधीजी ने 3 जनवरी, 1932 को पुन: सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने की घोषणा की। इस घोषणा के प्रत्युत्तर में विलिंगडन ने 4 जनवरी, 1932 को अचानक गांधीजी व सरदार पटेल को बन्दी बना लिया। इसके साथ ही अनेक कांग्रेसी नेताओं; जैसेशेरवानी, अंसारी, राजगोपालाचारी, पं. मदनमोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद आदि को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस से सम्बन्धित समाचार-पत्र व उसकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया गया। समस्त प्रकार के अत्याचारों व दमनकारी नीतियों के पश्चात् भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलता रहा।साम्प्रदायिक निर्णय व पूना समझौता -
इधर ब्रिटिश सरकार डॉ. अम्बेडकर व मुहम्मद अली जिन्ना से समझौता कर चुकी थी। डॉ. अम्बेडकर से समझौता हो जाने के कारण ही प्रधानमन्त्री मैक्डोनाल्ड ने सन् 1932 में अपने 'साम्प्रदायिक निर्णय' (मैक्डोनाल्ड निर्णय) की घोषणा की, जिसमें हरिजनों को पृथक् जाति मानकर उनके लिए मुसलमानों की तरह पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। गांधीजी ने इसके विरुद्ध पूना जेल में आमरण अनशन किया और 'पूना समझौते के द्वारा उपर्युक्त निर्णय में से हरिजनों के पृथक् प्रतिनिधित्व को वापस ले लिया।तृतीय गोलमेज सम्मेलन (नवम्बर, 1932) -
नवम्बर, 1932 में भारत सचिव सेमुअल होर द्वारा लन्दन में तृतीय गोलमेज
सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 46 ऐसे भारतीय प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया था जो
सरकार के समर्थक अथवा उदारवादी थे। सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलने के कारण कांग्रेस के
अधिकांश नेता जेलों में थे,
अत: कांग्रेस ने
इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस प्रकार तीसरा गोलमेज सम्मेलनं भी असफल रहा। इस
सम्मेलन में कोई नई बात नहीं हुई, वरन् प्रथम दो सम्मेलनों की पुष्टि के साथ ही 24 दिसम्बर, 1932 को यह सम्मेलन
भी समाप्त हो गया।
सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति
8 मई,
1933 को गांधीजी ने हरिजनोद्धार कार्यक्रम के संचालन के लिए आत्म-शुद्धि हेतु 21 दिन का
व्यक्तिगत उपवास रखने की घोषणा की। इस उपवास का उद्देश्य सामाजिक होने के कारण
सरकार ने गांधीजी को रिहा कर दिया। इस समय गांधीजी ने 6 सप्ताह के लिए
सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित करने का परामर्श दिया व 12 जुलाई के
कांग्रेस के पूना में हुए अनौपचारिक सम्मेलन द्वारा आन्दोलन को स्थगित कर दिया
गया।
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के
स्थगन के पश्चात् गांधीजी ने वायसराय से मिलने का प्रयास किया, किन्तु उन्होंने
यह कहकर मिलने से इन्कार कर दिया कि जब तक. यह आन्दोलन पूर्णतया समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक वह कोई बात
नहीं करना चाहते। तब गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की घोषणा की, जिसके कारण
उन्हें पुन: गिरफ्तार कर लिया गया। 16 अगस्त को गांधीजी ने उपवास प्रारम्भ कर दिया। किन्तु
वल्लभभाई पटेल आदि अन्य नेता बन्द ही रहे। मई, 1934 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा
आन्दोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा 20 मई,
1934 को यह आन्दोलन पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, -
इस प्रकार सविनय अवज्ञा
आन्दोलन समाप्त हो गया। शीघ्र ही कांग्रेस पर लगे प्रतिबन्ध भी उठा लिए गए, किन्तु उसकी
सहयोगी संस्थाएँ व संगठन प्रतिबन्धित ही रहे।
· सविनय अवज्ञा आन्दोलन का राजनीतिक महत्त्व
(1) इस आन्दोलन के
माध्यम से गांधीजी ने जनता को अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने का नया मार्ग
दिखाया। करबन्दी, नशाबन्दी, सविनय अवज्ञा आदि
ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें थीं जिनके प्रभाव से सरकार परेशान हो गई।
(2) आन्दोलन काल की घटनाओं ने देश की राजनीति पर गम्भीर प्रभाव
डाला था। इस आन्दोलन की बढ़ती शक्ति के कारण ही सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन
बुलाने की घोषणा की थी।
(3) कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, जिसके कारण यह
सम्मेलन सफल नहीं हो सका। इससे यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ही भारत की एकमात्र
राष्ट्रीय संस्था है। उसके सहयोग के अभाव में कोई योजना सफल नहीं हो सकती।
(4) यह पहला आन्दोलन था जिसके कारण ब्रिटिश सरकार गांधीजी से
बराबरी के स्तर पर वार्ता करने को सहमत हुई। निःसन्देह गांधी-इरविन समझौता इसी
आन्दोलन का परिणाम था। माइकल ब्रेचर के शब्दों में "वायसराय का वार्ता के लिए
राजी होना इस बात का प्रतीक था कि सरकार कांग्रेस को भारतीय जनता की प्रतिनिधि
संस्था मानती थी। यह गांधीजी की महान् सफलता थी।"
(5) यद्यपि यह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया था, तथापि यह सत्य है
कि सरकार भारतीय समस्याओं पर विचार करने के लिए विवश हो गई। सन् 1935 का भारत सरकार
अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत प्रदत्त प्रान्तीय स्वशासन की व्यवस्था इसी आन्दोलन की
देन थी।
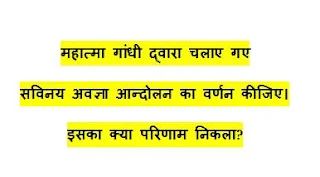
Comments
Post a Comment