तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परम्परागत दृष्टिकोण
प्रश्न 4. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परम्परागत उपागमों का वर्णन कीजिए।
उत्तर - तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का प्रारम्भ अरस्तू के समय से माना जाता है। अरस्तू ने अपने समय में प्रचलित विश्व के 158 संविधानों का अध्ययन करके संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो तुलनात्मक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। परम्परागत उपागमों के आधार पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वानों में अर्नेस्ट बार्कर, हैरॉल्ड लास्की, कार्ल जे. फ्रेड्रिक, हरमन फाइनर, ऑग व जिंक, मुनरो आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग कर यूरोप की संवैधानिक संस्थाओं की तुलनात्मक व्याख्या की।
तुलनात्मक
राजनीति के परम्परागत उपागम तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख परम्परागत उपागम
निम्नलिखित हैं -
(1) दार्शनिक उपागम–
राजनीतिशास्त्र
के अध्ययन का यह सबसे प्राचीन उपागम है। प्लेटो, थॉमस मूर,
बेकन, रूसो, काण्ट,
हीगल, ग्रीन, बोसॉके,
जे. एस. मिल आदि विद्वानों ने इस उपागम को अपनाया। प्लेटो
के ग्रन्थ 'The
Republic' में वर्णित दार्शनिक शासक और आदर्श राज्य की अवधारणा, मूर के ग्रन्थ 'Utopia' में वर्णित स्वर्गिक राज्य
की धारणा, लॉक की पुस्तक 'Two Treatises on
Government' में वर्णित प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार की
धारणा और रूसो की 'Social Contract' में वर्णित
सामान्य इच्छा को धारणा इसी उपागम के उदाहरण हैं। इस उपागम के अन्तर्गत राजनीतिक
जीवन के आदर्शों को निश्चित कर राजनीति को नैतिकता के उच्च नियमों के साथ जोड़
दिया जाता है।
(2) ऐतिहासिक उपागम–
राजनीतिक
संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता, वरन् वे विकास का परिणाम
होती हैं। अतः प्रत्येक राजनीतिक संस्था का एक अतीत होता है और उस अतीत से परिचित
होकर ही उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए राजनीति
विज्ञान में ऐतिहासिक उपागम का बहुत अधिक महत्त्व है। ऐतिहासिक उपागम की उपयोगिता
के कारण ही अरस्तू के समय से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। लास्की,
हीगल, मैकियावली, मॉण्टेस्क्यू,
कार्ल मार्क्स, हरबर्ट स्पेन्सर, मैक्स वेबर, कॉम्टे आदि
विद्वानों ने किसी-न-किसी रूप में इस उपागम का प्रयोग किया है।
ऐतिहासिक
उपागम हमें अतीत में देखने में सहायता प्रदान करता है और अतीत को समझकर वर्तमान से
तुलना करते हुए भविष्य के लिए मार्ग निकाला जा सकता है। ऐतिहासिक उपागम प्राचीन
राजनीतिक संस्थाओं,
प्रणालियों और आदर्शों को समझने में बहुत सहायक है।
(3) सांस्थानिक उपागम—
इसमें
अध्ययनकर्ता व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि राजनीतिक
संगठनों की औपचारिक संरचना पर बल देता है। अरस्तू से लेकर पोलिबियस तक और आधुनिक
काल में लॉर्ड ब्राइस, फाइनर आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं
में इस उपागम का प्रयोग किया है। आधुनिक विचारकों ने दल प्रणाली और हित समूहों को
भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। वाल्टर, बेजहाट,
ऑग, मुनरो, लास्की,
सी. एफ. स्ट्रांग, सारटोरी आदि विद्वानों ने भी अपनी रचनाओं में इस उपागम को अपनाया है।
(4) कानूनी उपागम-
19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक उपागम की प्रतिक्रिया स्वरूप कानूनी उपागम
अस्तित्व में आया। इस समय कुछ ऐसे विचारक सामने आए जिन्होंने राजनीतिक संस्थाओं पर विशुद्ध कानूनी
दृष्टिकोण से विचार किया डायसी, थियोडोर वुल्से, वुडरो विल्सन, कार्टर, हर्ज, न्यूमैन आदि विद्वानों ने विज के अनेक देशों की कानूनी संहिताओं और
संविधानों का विश्लेषण करने तुलनात्मक राजनीति को पुष्ट किया।
(5) समस्यागत उपागम-
इस उपागम के द्वारा समस्याग्रस्त
क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है । इस उपागम के द्वारा अनेक विद्वानों ने शासन
प्रणालियों की प्रचलित समस्याओं; जैसे-लोकतन्त्र तथा आर्थिक नियोजन में सम्बन्ध.
द्विसदनात्मक व्यवस्था का ह्रास, प्रदत्त व्यवस्थापन आदि का
अध्ययन कर सुझाव भी प्रस्तुत किए।
(6) क्षेत्रीय उपागम-
इस उपागम का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् हुआ। यह उपागम भौगोलिक समीपता को 'क्षेत्र' के निर्धारण का आधार मानता है। इस उपागम के आधार पर अनेक विद्वानों ने विकासशील देशों का अध्ययन किया। क्षेत्रीय उपागम के आधार पर लिखे गए ग्रन्थों में आमण्ड एवं कोलमैन की पुस्तक 'The Politics of Developing Areas', डेविस की पुस्तक 'Government and Politics in South East Asia', हरारी की पुस्तक 'Government and Politics of Middle East' आदि उल्लेखनीय हैं।
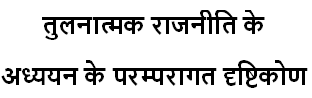
Comments
Post a Comment